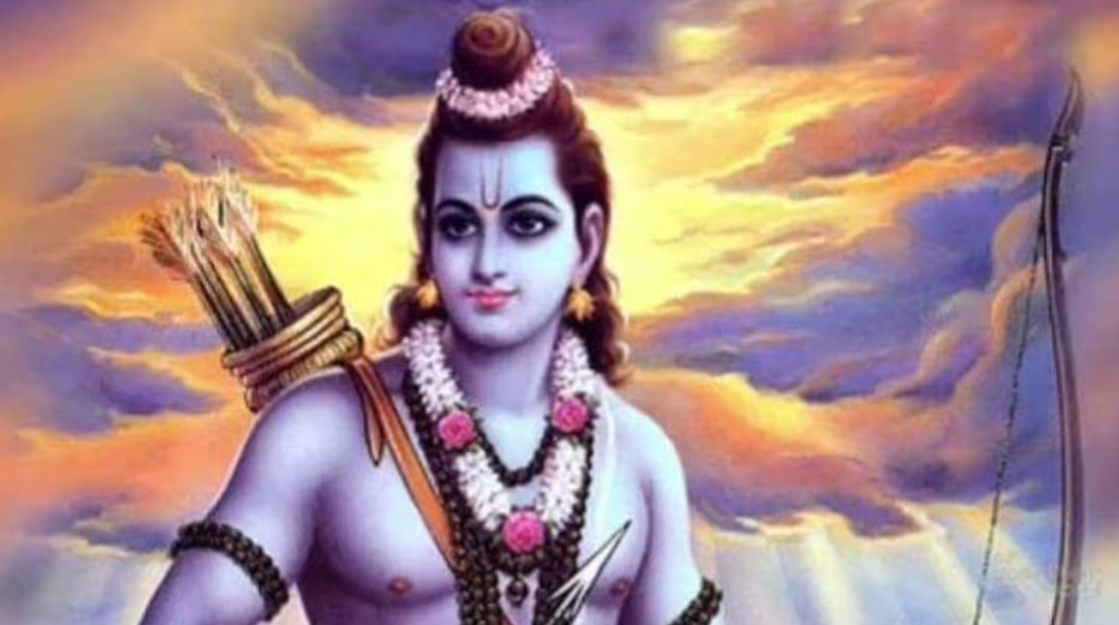रामनवमी का उल्लास भारत सहित दुनियाभर के कई देशों में दिखता है। राम की लोकप्रियता संदेह से परे है। जगह-जगह निकलने वाली राम की अनूठी झांकियां, जुलूस, स्वांग आदि यह साबित करते हैं। राम की इस जनस्वीकृति के पीछे भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक संरचना के अलावा लोककलाओं में उनकी मौजूदगी है। इसमें रामलीला बेहद महत्वपूर्ण है। लीला में चमत्कार तत्त्व प्रबल होता है। चमत्कार लोक को लुभाता है। रामलीला कला का जनतांत्रिक आस्वाद है। इसमें थोड़ा शास्त्र, थोड़ा रस है और ढेर सारा लोक व चमत्कार है। राम की छवि हथियार के साथ है।
धनुष उन्हें लोकरक्षक के रूप में प्रतिबिंबित कर रहा होता है। रामचरितमानस की रचना के साथ ही काशी में तुलसीदास ने रामलीला की शुरुआत की। उनकी कोशिश रही कि ‘मर्यादापुरुषोत्तम’ राम की छवि को अधिकाधिक लोकपरक बनाया जाय। रामलीला इसकी अहम कड़ी रही। रामलीला मूलतः वैष्णव आस्था तंत्र से जुड़ी है। जो सगुण भक्ति की उपासना पद्धति से प्रभावित है। यह अवतारवाद की संकल्पना से संबंधित है। राम की कथा कहने की परंपरा बाल्मीकि से भी पुरानी है। तुलसीदास ने राम की कथा रामचरितमानस के काफी पहले से शुरू कर दी थी। उनकी पहली रचना ‘रामललानहछू’ राम की कथा ही है।
रामचरितमानस पांचवी कृति थी। इसे प्रबंधात्मक रूप देते हुए भी उन्हें यह प्रतीत होता रहा कि राम के जिस जनतंत्रीकरण का वो प्रयास कर रहे हैं, वह कथावाचन मात्र से संभव नहीं है। जिसको संबोधित कर रहे हैं, उसे भी इस कथा का हिस्सा होना चाहिए। रामलीला की लोकप्रियता पर राम का जननायक रूप निखरता है। तुलसी ने रामलीला का आयोजन शरद ऋतु की शुरुआत में रखने का प्रावधान किया। यह समय उत्तर भारत में फसलों की कटाई का होता है। इसमें गांव और परिवार के लोगों का सामूहिक श्रम लगता है। इस सामूहिक श्रम की विश्रांति सामूहिक सांस्कृतिक कर्म में ही हो सकती है।
खेती-किसानी करने वाला परिवार एकजुट रहे, इसके लिए पारिवारिक मूल्यों को महसूस कराने वाली रामलीला सहज ही स्वीकार होती गई। अयोध्या का ठाठ-बाट और धन-वैभव भोग से ज्यादा त्याग का प्रतीक था। पूरा परिवार श्रम करता था खेती-किसानी में लेकिन उपभोग कोई एक ही नहीं करता था, सबके लिये सबकुछ था। बिल्कुल परंपरागत अर्थों में उत्तर भारतीय ग्रामीण परिवार की निर्मिति और इस निर्मिति को संभव कराने वाले मूल्यों को संरक्षित और प्रदर्शित करने वाली रामकथा रामलीला में जीवंत हो उठती है। वैसे भी सीता सुकुमारी खेत से निकली थीं, यह तथ्य किसानी संस्कृति की भावनाओं को कितना छूता होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। रामलीला से तुलसी ने हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता की जमीन बनाई।
रामचरितमानस की रचना भले ही प्रयाग में शुरू की थी लेकिन पूरा किया बनारस में आकर। बनारस सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि भौगोलिक रूप से भी एक संवेदनशील स्थान था। गंगा बनारस के केन्द्र में हैं। गंगा के पूरब दिशा में बहाव के साथ तुलसी और उनकी रामलीला के बहाव को भी देखा जा सकता है। काशी, वाराणसी और बनारस का अपना राजनीतिक समाजशास्त्र तो है ही, भौगोलिक भी है। जिस स्थान को काशी कहा जाता है, उसके ठीक सामने की बसाहट का नाम कज्ज़ाकपुरा है। यहाँ कसाईबाड़े की ऐतिहासिक मौजूदगी रही है। तुलसी ने पहले यहीं रामलीला शुरू कराई। दूसरा स्थान चुना रामनगर।
रामनगर के ठीक पड़ोस की जगह का नाम है- पड़ाव। यहाँ मुगलिया सैन्य छावनी थी। इसके ठीक पूरब में तो बकायदा मुगलसराय ही था। फिर गंगा की धारा के किनारे-किनारे पूरब की तरफ बढ़ते चले जायें, और रामलीला के आरंभ काल और इसकी क्रमशः बढ़ती लोकप्रियता को पहचानने की कोशिश करते जायें, तो तस्वीर गंगासागर से काफी पहले ही साफ-साफ दिखने लगती है। रामलीला एक नाट्यशैली है। नाटक मशीनों और तकनीकि साधनों के हावी होने से पहले की सर्वाधिक लोकप्रिय और लोकतांत्रिक विधा रही है क्योंकि इसमें नट और दर्शक प्रत्यक्ष होते हैं। अक्सर परिचित भी।
रामलीला चूंकि तत्कालीन नगरीय संरचना से निकलकर ग्रामीण संरचना की तरफ अधिक बढ़ रही थी, इसलिए इसके पात्र प्रायः परिचित या संबंधी हुआ करते थे। रामलीला के पात्र गंवई गांव के किसान और मेहनतकश लोग बनते रहे हैं। प्रेमचंद की कहानी ‘रामलीला’ को इस संदर्भ में फिर से पढ़ा जाना चाहिए। तुलसी ने रामलीला के पात्रों के रूप में इस वर्ग का चुनाव करके ऐतिहासिक कार्य किया। पहली बार रामादि का मुकुट या वेश धारण करते हुए किसी लल्लन तिवारी या किसी नथुनी सिंह ने खुद को ‘ईश्वर’ के रूप में पाया होगा। अपने ही लोगों से आदर और श्रद्धा पाते हुए खुद को गौरवान्वित और आर्द्र महसूस किया होगा।
‘प्रभु श्रीराम’ संस्कृत और मंदिर से बाहर भी मिल सकते हैं, हमारे बीच हो सकते हैं, हममें हो सकते हैं, यह अनुभव तुलसी के इस सांस्कृतिक उद्यम ने कराया होगा और इस तरह राम के जननायक के तौर पर रूपांतरण में रामलीला ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई।रामलीला एक ऐसे कलारूप के तौर पर विकसित हुई जिसमें आर्थिक निवेश या उत्पादन की लागत न्यूनतम थी। किसी विशेष किस्म के रंगमंच की जगह गांवों में मंदिर के प्रांगण या साझा चबूतरों पर घर की ही धोती को धोकर, हल्दी से रंगकर पर्दे और कनात तैयार किये जाते थे। रौशनी के लिए सब मिलकर अपने घरों से दिये, मशालें और आगे चलकर पेट्रोमैक्स की व्यवस्था कर लिया करते थे।
दर्शकों को कुर्सी नहीं चाहिये थी। अपने-अपने घरों से टाट-दरी लाकर बिछाना और लौटते वक्त समेटकर ले जाना, अलग ही आनंद देता था। रामलीला की शुरुआत का समय प्रायः देर शाम हुआ करता है। ग्रामीण व्यवस्था में सूरज ढलने के बाद पुरुष भी श्रम के कार्यों से विरत होते हैं और स्त्रियां भी चूल्हे-चौके से निपट चुकी होती हैं। ऐसे में परिवार के साथ जाकर ‘लीला’ देखने का यह सुख, मध्ययुगीन भारत में स्त्री-मुक्ति का क्षणिक ही सही लेकिन एक अवसर तो था ही। रामलीला को आगे बढ़ाने वाले व्यासजी, रेवड़ी और बदाम का ठेला लगाने वाले चच्चा और न जाने कितने अपने लोग इस नाट्यरूप के निवेश थे।
उत्पादन की प्रक्रिया की ऐसी लोकतांत्रिक भागीदारी अन्यत्र दुर्लभ है। इस कलारूप का परिशंसन जिनके बीच होना था, वे भी किसी कीमत की अपेक्षा नहीं करते। यानि रचना (उत्पाद) और बाजार (दर्शक) के बीच व्यावसायिक न होकर शौकिया और आत्मीय रिश्ता इसे आश्चर्यजनक ढंग से लोकप्रिय बनाता है। रामलीला का कथा-आधार प्रायः तुलसीकृत रामचरितमानस ही है। ध्यान रहे कि तमाम धर्मग्रंथों साथ-साथ रामचरितमानस को जन-जन तक पहुंचाने वाले गीताप्रेस की स्थापना भी 1928 में हुई थी। इसलिए रामलीला के संवादों को प्रचारित-प्रसारित करने में तुलसीदास और उनके शिष्यों ने कितना श्रम किया होगा, यह अनुमान से भी परे है।
बनारस और इसके आसपास के क्षेत्रों में ‘रामचरितमानस’ के आधार पर होने वाली रामलीला में अवधी की शब्दावली से दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मानस के बाद के संस्करणों में अवधी के साथ-साथ भोजपुरी और उर्दू के शब्द भी मिलते हैं। इसमें कुछ योग तुलसी की बनारस से प्रभावित अवधी भाषा का है तो कुछ योग गीता-प्रेस का भी। इन क्षेत्रों में रामलीला के संवादों के लिए ‘रामचरितमानस दर्पण’ और ‘राधेश्याम रामायण’ का प्रयोग बाद में होने लगा। रामलीला को लोकप्रिय बनाने में राधेश्याम कथावाचक की संवाद-योजना का ऐतिहासिक योगदान रहा है।
उर्दू और खड़ी बोली हिन्दी का ऐसा बहनापा, जबकि कई सारे स्थापित संपादक, समीक्षक हिन्दी का सही ढब खोज रहे थे, अपने आप में आईना दिखाने जैसा है। कथावाचक संस्कृत, फारसी, हिन्दी, थियेटर और सिनेमा के नागरिक थे। उन्होंने रामलीला में अपने संवादों के जरिये अद्भुत ढंग से नाटकीयता भर दी। उर्दू के शब्दों का कुछ तो असर था कि अभी तक कटा-कटा सा गैर हिन्दू समाज भी रामलीला में रुचि लेने लगा था। यह शोध किया जाना चाहिए कि कौन से कारण थे कि तमाम टकराहटों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में रामलीला का शामियाना आज भी कोई सैयद अंसारी मुफ्त में देते हैं।
रामनवमी के जुलूस की लाल और केसरिया झंडियां आज भी किसी अब्दुल्ला टेलरिंग शॉप से ही सिलकर आती हैं और लंका जलाने में जो कपड़ा लगता है, वह यहीं की बची हुई कतरनें हैं। लक्ष्मण को शक्तिबाण लगने पर मिल्खी आपा कोने में आज भी ज़ार-ज़ार रोती हैं। परशुराम जिस चौकी पर अपना क्रोध अभिनीत कर रहे होते हैं, वह किसी इम्तियाज भाई ने साल-दर-साल इसी दिन के लिए संभाल रखी है। रावण के पुतले में जो खोपड़ी वाला हिस्सा है, उस पर मूंछ और भौहें काले पेंट से हैदर चचा अपनी कांपती अंगुलियों से बनाते चले आ रहे हैं। रामलीला ने हिन्दुस्तानी जातीयता को बनाने में भी काफी हद तक योगदान किया है, इसे बचाने की जरूरत है।
अंग्रेजों के विरोध में राम और अन्य साधु पात्रों की खादी और खल पात्रों की विदेशी पोशाकों के आशय को समझने की जरूरत है। रामलीला का समाजशास्त्रीय अध्ययन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विकास का गौरवगान करने के साथ-साथ स्थानीय और लघु राष्ट्रीयताओं की आवाजों को सुनने की सहूलियत भी देता है।

लेखक: डॉ. अविनाश कुमार सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषा विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
READ ALSO: रामनवमी : श्रीश्री बाल मंदिर अखाड़ा की शोभायात्रा में इंदौर की झांकी का रहेगा आकर्षण