नयी दिल्ली। भारत का महत्वाकांक्षी आदित्य-एल1 मिशन अंतरिक्ष-आधारित सौर अध्ययन में देश के शुरुआती प्रयास का प्रतीक है और यह सूर्य की गतिविधियों और पृथ्वी पर उनके प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह बात विशेषज्ञों ने कही। देश के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों ने तब एक महत्वपूर्ण छलांग लगायी है, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शनिवार को सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए सात पेलोड के साथ अपने पहले सौर मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।
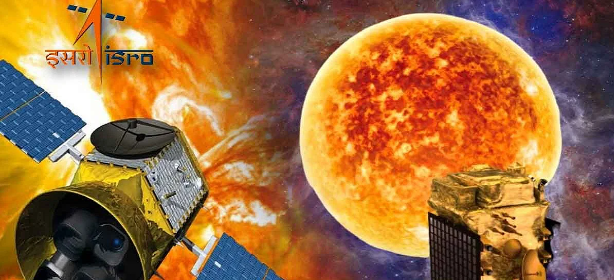
सूर्य के अध्ययन के लिए बेहद अहम है आदित्य-एल1 मिशन
कई विशेषज्ञों ने मिशन के सफल प्रक्षेपण और विज्ञान एवं मानवता के लिए इसके महत्व की सराहना की। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता में अंतरिक्ष विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र के प्रमुख दिव्येंदु नंदी ने कहा कि यह मिशन सूर्य के अंतरिक्ष-आधारित अध्ययन में भारत का पहला प्रयास है।
यदि यह अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदु एल1 तक पहुंचता है, तो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो वहां सौर वेधशाला स्थापित करने वाली तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन जाएगी। अंतरिक्ष यान 125 दिनों में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, लैग्रेंजियन बिंदु एल1 के आसपास प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किए जाने की उम्मीद है, जिसे सूर्य के सबसे करीब माना जाता है।
सूर्य मिशन को ‘आदित्य एल-1’ नाम क्यों दिया गयाा :
वैज्ञानिकों के मुताबिक, पृथ्वी और सूर्य के बीच पांच ‘लैग्रेंजियन’ बिंदु (या पार्किंग क्षेत्र) हैं, जहां पहुंचने पर कोई वस्तु वहीं रुक जाती है। लैग्रेंज बिंदुओं का नाम इतालवी-फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ-लुई लैग्रेंज के नाम पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले उनके अनुसंधान पत्र-‘एस्से सुर ले प्रोब्लेम डेस ट्रोइस कॉर्प्स, 1772’ के लिए रखा गया है। लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी जैसे आकाशीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एक कृत्रिम उपग्रह पर केन्द्राभिमुख बल के साथ संतुलन बनाते हैं। सूर्य मिशन को ‘आदित्य एल-1’ नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु1 (एल1) क्षेत्र में रहकर अपने अध्ययन कार्य को अंजाम देगा।

अंतरिक्ष पर्यावरण की निगरानी के साथ अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में मिलेगी मदद :
नंदी ने बताया कि लैग्रेंज बिंदु एल1 के पास रखा गया कोई भी उपग्रह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा, जिससे चंद्रमा या पृथ्वी द्वारा कोई बाधा उत्पन्न किये बिना इसके द्वारा सूर्य का निर्बाध अवलोकन किया जा सकेगा। नंदी ने कहा कि अंतरिक्ष के मौसम में सूर्य-प्रेरित परिवर्तन पृथ्वी पर प्रभाव डालने से पहले एल1 पर दिखाई देते हैं, जो पूर्वानुमान के लिए एक छोटी, लेकिन महत्वपूर्ण खिड़की प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि आदित्य-एल1 उपग्रह, एक सहयोगी राष्ट्रीय प्रयास है, जिसका उद्देश्य ‘कोरोनल मास इजेक्शन’ (सीएमई) सहित सूर्य की गतिविधि के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना है। यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष पर्यावरण की भी निगरानी करेगा और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान मॉडल को परिष्कृत करने में योगदान देगा।
गंभीर अंतरिक्ष मौसम दूरसंचार और नौवहन नेटवर्क, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो संचार, ध्रुवीय मार्गों पर हवाई यातायात, विद्युत ऊर्जा ग्रिड और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों पर तेल पाइपलाइनों को प्रभावित करता है।
मिशन, सूर्य के असाधारण कोरोना के रहस्यों को करेगा उजागर :
अशोक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमक राय चौधरी इस बात पर जोर देते हैं कि यह मिशन वैज्ञानिक जिज्ञासा से परे है, क्योंकि इसका उद्योग और समाज पर प्रभाव है। पूर्व में इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए), पुणे के निदेशक रहे रायचौधरी ने कहा कि आदित्य-एल1 मिशन मुख्य रूप से वैज्ञानिक लक्ष्यों का पीछा करता है, लेकिन इसका प्रभाव उद्योग और समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं तक फैला हुआ है।
मिशन का उद्देश्य सूर्य के असाधारण कोरोना के रहस्यों को उजागर करना है, जिसका तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि इसकी सतह अपेक्षाकृत ठंडी 5500 डिग्री सेल्सियस रहती है। रायचौधरी ने समझाया कि इनमें से निकलने वाले उच्च-ऊर्जा कण, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शंस कहा जाता है, पृथ्वी से टकराते हैं।
वे हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, जिन पर हम संचार, इंटरनेट और जीपीएस सेवाओं के लिए निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह अनुमान लगाने के साधन की आवश्यकता है कि ये सीएमई कब और कितनी तीव्रता से घटित होंगे। आदित्य-एल1 हमें अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए ज्ञान प्रदान करेगा।
इसके अतिरिक्त, मिशन का उद्देश्य यह समझना है कि सूर्य की सतह पर सौर तूफान कैसे उच्च-ऊर्जा चार्ज कण उत्पन्न करते हैं, जो संभावित रूप से उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे आधुनिक जीवन के तरीके को बाधित कर सकते हैं। रायचौधरी ने कहा कि ये दोनों मुद्दे संभवतः जुड़े हुए हैं और आदित्य-एल1 के दो प्रमुख उपकरण, पराबैंगनी कैमरा और कोरोना स्पेक्ट्रोग्राफ, संबंध का पता लगाने के लिए एक साथ सूर्य का निरीक्षण करेंगे।
खगोलभौतिकीविद् संदीप चक्रवर्ती ने पिछले कुछ वर्षों में मिशन के विकास पर प्रकाश डाला।

भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी केंद्र के निदेशक ने रखी अपनी राय :
कोलकाता स्थित भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी केंद्र के निदेशक चक्रवर्ती ने बताया कि आदित्य की संकल्पना 15 साल से भी पहले की गई थी, शुरू में यह सौर कोरोना के आधार पर प्लाज्मा वेग का अध्ययन करने के लिए था। बाउ में यह यह आदित्य-एल1 और फिर आदित्य एल1+ के तौर पर विकसित हुआ, अंततः उपकरणों के साथ आदित्य-एल1 में वापस आ गया। चक्रवर्ती ने मिशन के उपकरणों और क्षमताओं के बारे में भी जानकारी दी। उनके अनुसार, पेलोड थोड़ा निराशाजनक रहा है और उपग्रह निश्चित रूप से खोज श्रेणी एक का नहीं है।
उन्होंने कहा कि लगभग सभी उपकरण लगभग 50 साल पहले नासा द्वारा भेजे गए थे, उदाहरण के लिए 1970 के दशक की शुरुआत में पायनियर 10, 11 आदि में। साथ ही सुरक्षित रहने के लिए, ताकि सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से उपकरण क्षतिग्रस्त न हों, ब्लॉकिंग डिस्क का आकार बहुत बड़ा है, जो सौर डिस्क से लगभग पांच प्रतिशत बड़ा है। इसलिए यह सौर सतह से केवल 35,000 किलोमीटर की दूरी पर ही वेग माप सकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, वैज्ञानिक ने कहा कि आदित्य-एल1 मिशन में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान के मामले में नासा की बराबरी करने के लिए भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है। नंदी ने कहा कि वैज्ञानिकों को आदित्य-एल1 को क्रियाशील देखने और मिशन की समग्र सफलता का आकलन करने के लिए लगभग चार महीने इंतजार करना होगा।
सौर अन्वेषण : महत्वपूर्ण वैश्विक मिशनों की एक दौड़ :
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अपने पहले सौर मिशन आदित्य-1 के सफल प्रक्षेपण की पृष्ठभूमि में, आइए हम दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के उन प्रमुख मिशन के माध्यम से इसे जानने का प्रयास करें, जो सूर्य के गूढ़ रहस्य को सुलझाने के लिए समर्पित हैं।
अमेरिका: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने अगस्त 2018 में पार्कर सोलर प्रोब का प्रक्षेपण किया था। दिसंबर 2021 में, पार्कर ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल ‘कोरोना’ से उड़ान भरी और वहां कणों और चुंबकीय क्षेत्रों की जानकारी लेने का प्रयास किया।
नासा के अनुसार, यह पहली बार था कि किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य से संबंधित पहलुओं का अध्ययन किया। नासा ने फरवरी 2020 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के साथ हाथ मिलाया और डेटा एकत्र करने के लिए ‘सोलर ऑर्बिटर’ का प्रक्षेपण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सूर्य ने पूरे सौर मंडल में लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण को कैसे निर्मित और नियंत्रित किया।
नासा की ओर से अन्य सक्रिय सौर मिशन में अगस्त, 1997 में प्रक्षेपित ‘एडवांस्ड कंपोज़िशन एक्सप्लोरर’, अक्टूबर, 2006 में प्रक्षेपित सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन्स ऑर्ब्जवेट्री; फरवरी, 2010 में प्रक्षेपित सोलर डायनेमिक्स वेधशाला; और जून 2013 में प्रक्षेपित इंटरफ़ेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ शामिल हैं। इसके अलावा, दिसंबर, 1995 में नासा, ईएसए और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जेएएक्सए) ने संयुक्त रूप से सोलर एंड हेलिओस्फेरिक ऑब्ज़र्वेटरी (एसओएचओ) का प्रक्षेपण किया था।
जापान : जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जेएएक्सए ने 1981 में अपना पहला सौर प्रेक्षण उपग्रह, हिनोटोरी (एस्ट्रो-ए) प्रक्षेपित किया। जेएएक्सए के अनुसार, इसका उद्देश्य कठोर एक्स-रे का इस्तेमाल करके सौर ज्वालाओं का अध्ययन करना था। जेएएक्सए के अन्य सौर अन्वेषण मिशन में 1991 में प्रक्षेपित योहकोह (सोलर-ए), 1995 में प्रक्षेपित एसओएचओ (नासा और ईएसए के साथ); और 1998 में नासा के साथ ट्रांजिएंट रीजन एंड कोरोनल एक्सप्लोरर (ट्रेस) शामिल हैं।
वर्ष 2006 में, हिनोड (सोलर-बी) लॉन्च किया गया था, जो परिक्रमा करने वाली सौर वेधशाला योहकोह (सोलर-ए) का उत्तराधिकारी था। जापान ने इसे अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर प्रक्षेपित किया था। हिनोड का उद्देश्य पृथ्वी पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करना है।
योहकोह का उद्देश्य सौर ज्वालाओं और सौर कोरोना का निरीक्षण करना था। जेएएक्सए की वेबसाइट के अनुसार, यह लगभग पूरे 11 साल के सौर गतिविधि चक्र को ट्रैक करने वाला पहला उपग्रह था।
यूरोप: अक्टूबर, 1990 में, ईएसए ने सूर्य के ध्रुवों के ऊपर और नीचे अंतरिक्ष के पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए यूलिसिस का प्रक्षेपण किया, जिससे वैज्ञानिकों को सूर्य के आसपास के अंतरिक्ष पर पड़ने वाले परिवर्तनशील प्रभाव के बारे में जानकारी मिली। नासा और जेएएक्सए के सहयोग से प्रक्षेपित विभिन्न सौर मिशन के अलावा, ईएसए ने अक्टूबर, 2001 में प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनोमी (प्रोबा)-2 प्रक्षेपित किया। प्रोबा-2, प्रोबा शृंखला का दूसरा मिशन है, जो लगभग आठ वर्षों के प्रोबा-1 के सफल अनुभव पर आधारित है। यह बात और है कि प्रोबा-1 सौर अन्वेषण मिशन नहीं था। ईएसए के आगामी सौर मिशनों में 2024 के लिए निर्धारित प्रोबा-3 और 2025 के लिए निर्धारित स्माइल शामिल हैं।
चीन: एडवांस्ड स्पेस-बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेट्री (एएसओ-एस) को नेशनल स्पेस साइंस सेंटर, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज (सीएएस) द्वारा अक्टूबर, 2022 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, एएसओ-एस मिशन को सौर चुंबकीय क्षेत्र, सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) के बीच संबंधों की जानकारी हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सौर ज्वालाएं और सीएमई विस्फोटक सौर घटनाएं हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित होती हैं।
इसरो चंद्र और सूर्य मिशन के बाद अंतरिक्ष की समझ बढ़ाने के लिए अन्य परियोजना के लिए तैयार :
चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारने के एक पखवाड़े से भी कम समय में सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए ‘आदित्य-एल1’ को रवाना करने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अब अंतरिक्ष की समझ को और बढ़ाने के लिए अन्य परियोजना के साथ तैयार है।
एक्पोसैट (एक्सर रे पोलारिमीटर सैटेलाइट) भारत का पहला समर्पित पोलारिमेट्री मिशन है जो कठिन परिस्थितियों मे भी चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों के विभिन्न आयामों का अध्ययन करेगा। इसके लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा जिसमें दो वैज्ञानिक अध्ययन उपकरण (पेलोड) लगे होंगे।
इसरो ने बताया कि प्राथमिक उपकरण ‘पोलिक्स’ (एक्सरे में पोलारिमीटर उपकरण) खगोलीय मूल के 8-30 केवी फोटॉन की मध्यम एक्स-रे ऊर्जा रेंज में पोलारिमेट्री मापदंडों (ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण) को मापेगा। इसरो के अनुसार, ‘एक्सस्पेक्ट’ (एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग) पेलोड 0.8-15 केवी की ऊर्जा रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपिक (भौतिक विज्ञान की एक शाखा जिसमें पदार्थों द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन से पदार्थों की आंतरिक रचना का ज्ञान प्राप्त किया जाता है) की जानकारी देगा।
इसरो के एक अधिकारी ने बेंगलुरु स्थित मुख्यालय में कहा कि एक्सपोसैट प्रक्षेपण के लिए तैयार है। इसने कहा कि ब्लैकहोल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक, पल्सर पवन निहारिका जैसे विभिन्न खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन तंत्र जटिल भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है और इसे समझना चुनौतीपूर्ण है।
अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि हालांकि विभिन्न अंतरिक्ष-आधारित वेधशालाओं द्वारा प्रचुर मात्रा में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी प्रदान की जाती है, लेकिन ऐसे स्रोतों से उत्सर्जन की सटीक प्रकृति को समझना अभी भी खगोलविदों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसरो ने कहा, ‘‘पोलारिमेट्री माप हमारी समझ में दो और आयाम जोड़ते हैं, ध्रुवीकरण की डिग्री और ध्रुवीकरण का कोण और इस प्रकार यह खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने का एक उत्कृष्ट तरीका है।
READ ALSO : Aditya L-1 हुआ Launch: भारत का पहला सूर्य मिशन, जानिए क्यों खास



